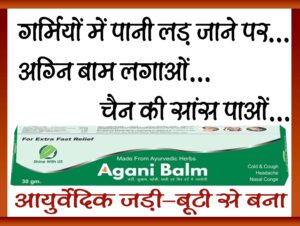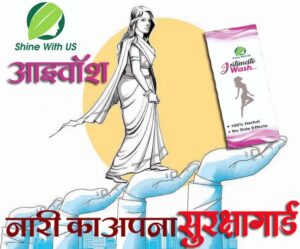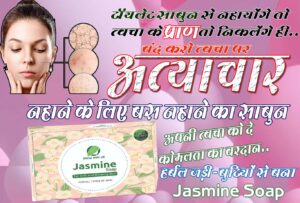किसी शहर में एक सेठ रहता था। उसके पास अपार धन-संपत्ति थी। समाज में उसकी अच्छी-खासी प्रतिष्ठा भी थी, पर उसका मन सदैव अशांत रहता था। सब कुछ होने पर भी उसे अपने भीतर खालीपन महसूस होता था। एक दिन उसे पता चला कि शहर के बाहर एक महात्मा आए हैं। अगले ही दिन वह उनके पास जा पहुंचा। महात्मा को प्रणाम कर सेठ बोला, ‘महाराज, मैं जीवन भर धन-संपत्ति अर्जित करने के लिए मेहनत करता रहा। सफलता भी मिली, मगर मुझे हमेशा अपनी संपत्ति और प्रतिष्ठा खो जाने का डर सताता रहता है। कोई ऐसा रास्ता बताएं कि मैं खुश और संतुष्ट रह सकूं।’
सेठ की मनोदशा समझते हुए महात्मा बोले, ‘शहर में एक व्यापारी है, तुम जाकर उससे मिलो। वही तुम्हें जीवन की सही राह सुझाएगा।’ यह सुन सेठ मायूस हो गया। उसने सोचा, ‘जब इतने पहुंचे हुए महात्मा कुछ नहीं समझा पा रहे तो वह साधारण सा व्यापारी क्या बताएगा।’ फिर भी खिन्न मन से वह व्यापारी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। व्यापारी हतप्रभ था। वह बोला, ‘मेरे पास बताने को कुछ नहीं है। मैं तो ग्राहकों को सौदा तौलकर देता हूं। बस इतना ही ध्यान रहता है कि तौलते समय तराजू का कांटा एकदम बीच में रहे।’
असंतुष्ट सेठ एक बार फिर महात्मा के पास गया और अपना क्रोध दबाते हुए निराशा भरे स्वर में बोला, ‘उस व्यापारी को कोई ज्ञान नहीं है, मैं बेकार अपना समय बर्बाद कर रहा हूं।’ महात्मा मुस्कराए और बोले, ‘तुमने व्यापारी की बात का अर्थ नहीं समझा। उसने तो जीवन की कुंजी बताई थी। असल में वह मध्यमार्ग की बात कर रहा था।’
जीवन-मृत्यु, सुख-दुख, क्रोध-करुणा, भोग-त्याग इत्यादि जीवन के दो छोर हैं। मृत्यु एवं दुख को हम नकारते हैं जबकि जीवन और सुख का स्वागत करते हैं। कोई भोग में लिप्त है तो कोई त्याग की प्रतिमूर्ति बनना चाहता है। इस तरह किसी एक ध्रुव के प्रति लगाव हमारे संतुलन को बिगाड़ देता है। जीवन वास्तव में घड़ी के पेंडुलम की तरह है, जो बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं गतिशील रहता है, पर उसकी स्थिर अवस्था हमेशा मध्य में होती है। हमारा जीवन भी सुख-दुख, जीवन-मृत्यु रूपी एक छोर से दूसरे छोर तक एक प्रवाह है। जीवन के दोनों पहलुओं, दोनों छोरों को एक साथ न देख पाने के कारण वे हमें अलग-अलग मालूम होते हैं, जबकि वास्तव में वे दोनों एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं।
यदि हम मध्य में रहें तो हम दोनों छोर एक साथ देख पाएंगे और यह बोध हो सकेगा कि अपोजिट दिखने वाले दोनों छोर दरअसल एक ही चीज का फैलाव हैं। इस तरह दोनो छोरों की स्वीकार्यता ही मध्यमार्ग है। इस स्वीकार्यता में हम संतुलन में होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रस्सी पर चलने वाला नट मध्य में रह कर रस्सी के बाई और दाईं तरफ झुकता है और अपना संतुलन बनाए रखता है। मध्य में रहने से हम लचीले हो जाते हैं। हमारी दृष्टि सम्यक हो जाती है। हम बाहर और भीतर दोनों तरफ देख पाते हैं। हम सफलता के बजाय सार्थकता की तलाश में लग जाते हैं। चित्त द्वंद्व से मुक्त हो तनावरहित हो जाता है। मध्यमार्ग पर चलने वाला फूल एवं कांटों को एक ही सिक्के के दो पहलू मानते हुए फूल को उसकी समग्रता में स्वीकार करता है।